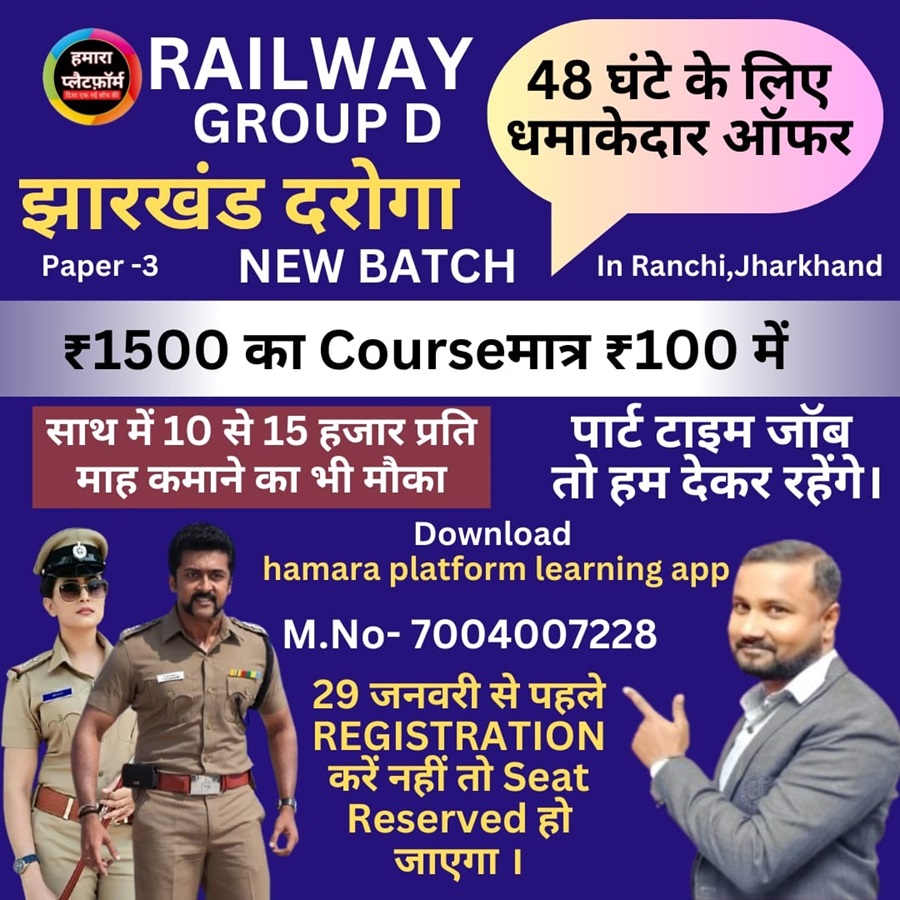सुधीर पाल
मेरे एक मित्र ने टिप्पणी की है कि आप(मैं) गैर-आदिवासी हैं, आपको किसी आदिवासी संगठन ने पेसा पर बोलने को अधिकृत नहीं किया है, फिर आप किस हैसियत से पेसा पर बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 28 सालों के बाद भी पेसा नहीं लागू हो पाया है तो इसकी वजह भी यही भ्रांति है। यह भ्रांति केवल मेरे कुछ मित्रों को ही नहीं है, बल्कि राज्य के कई नीति-नियन्तकों और लाभ-हानि से राजनीतिक मसले पर काम करने वाले ज्यादातर राजनीतिक दलों और राजनेताओं को भी है। पेसा के बारे में आम भ्रांति है कि यह कानून सिर्फ आदिवासियों के लिए है। झारखंड के मूलवासियों-सदानों और अल्पसंख्यकों को भी लगता है कि इस कानून में उनके हितों की अनदेखी हुई है। मूलवासियों-सदानों को अंदेशा है कि पेसा लागू होने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुछ आदिवासी संगठनों और बुद्धिजीवियों द्वारा भी ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है। जबकि वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है।
संवैधानिक और कानूनी स्वरूप में पेसा बेहद समावेशी है। पेसा में समावेशी पंचायत की व्यवस्था है। ग्राम सभाएं सार्वभौमिक हैं और निर्णय में सामुदायिक चेतना की सर्वोच्चता है। पेसा का वास्ता अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों से है चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म और लिंग के ही क्यों ना हों? इस कानून का नाम ‘पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996’ है।

पेसा की बुनियाद इन चार महत्वपूर्ण प्रावधानों पर है:
पेसा 1996-4(ए): पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रुढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा; पेसा 1996-4(बी) ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो; पेसा 1996-4(सी) प्रत्येक ग्राम की एक ग्रामसभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नियमावलियों में सम्मलित किया गया है; पेसा 1996-4(डी) प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निबटाने के रुढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण के लिए सक्षम होगी;
इसमें दो राय नहीं कि पेसा कानून को ड्राफ्ट करने वाले लोग बेहद संवेदनशील थे और उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राउन्ड रियल्टी की बेहतर जानकारी थी। इसलिए पूरे कानून में सिर्फ ‘समुदायों की परंपरा’ की बात की गयी है, ना कि आदिवासियों की परंपरा। ‘समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों’ की बात की गयी है ना कि आदिवासियों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों की।
‘विवाद निबटाने के रुढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण’ की बात है ना कि सिर्फ ‘आदिवासियों के विवाद निबटाने के रुढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण’ की बात है। सनद रहे कि हर समुदाय चाहे आदिवासी हो या गैर-आदिवासी उसकी अपनी परंपरा है, उसकी सांस्कृतिक पहचान है और उसकी धार्मिक आस्था भी है। कोई भी समुदाय बिना परंपरा या सांस्कृतिक पहचान के जिंदा नहीं रहता है। इतना ही नहीं ग्राम सभाओं के मामले में भी समुदायों को यह स्वतंत्रता है।‘ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो;’। इसलिए इस मुगालते में नहीं रहा जाए कि पेसा में सिर्फ आदिवासियों के लिए जगह है या यह कानून सिर्फ आदिवासियों के लिए है। यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र के गांव में सिर्फ आदिवासी ही रहते हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक झारखंड के अनुसूचित जिलों के 922 गांव में आदिवासियों की आबादी 10 फीसदी से कम थी और 1658 गांव ऐसे थे जहां आदिवासियों की आबादी शून्य थी। 2011 की जनगणना में निश्चित तौर पर आबादी का यह आंकड़ा और भी कम् होगा।इन गांव में किन समुदायों की पारंपरिक व्यवस्था को स्वीकार्यता मिलनी चाहिए।
.jpeg)
पेसा कानून में सिर्फ तीन प्रावधान सीधे तौर पर अनुसूचित जनजाति से वास्ता रखते हैं।पेसा का 4(जी)- परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा;
परंतु यह और कि पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए रहेंगे।
इस कानून में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण दिए जाने संबंधी प्रावधानों में और धन उधार देने के संबंध में ही अनुसूचित जनजाति समुदाय की बात हुई है। बाकी सभी जगहों पर सिर्फ समुदायों की बात की गयी है।
ग्राम सभा का गठन गांव के वयस्कों से मिलकर होगी और किसी खास समुदाय या जाति विशेष से होने की कोई शर्त नहीं है। शर्त केवल यही है कि उस गांव की पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो। इन इलाकों के सभी स्तरों के पंचायत में सिवाय अध्यक्ष पद के (और आरक्षित सीटों) किसी भी समुदाय के लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सक्ने में सक्षम हैं। मतलब है कि ग्राम सभा या पंचायतों के निर्णय में आदिवासियों और गैर- आदिवासियों दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। झारखंड के गांव की डेमोग्राफी की बात करें तो ज्यादातर गॉवों में/ पंचायतों में बिना गैर आदिवासियों की सहमति के कोई भी प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाएगा।
झारखंड का सामाजिक ताना-बाना और सांस्कृतिक पहचान आदिवासियों,मूलवासियों-सदानों, अल्पसंख्यकों और दलितों की साझी संस्कृति से मिलकर बनी और यहाँ की मिट्टी में रची-बसी है। इसे बनाए और बचाए रहने की जिम्मेवारी हम सभी की है।
(नोट- इस आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। इनका द फॉलोअप से कोई लेनादेना नहीं है)